Breaking News
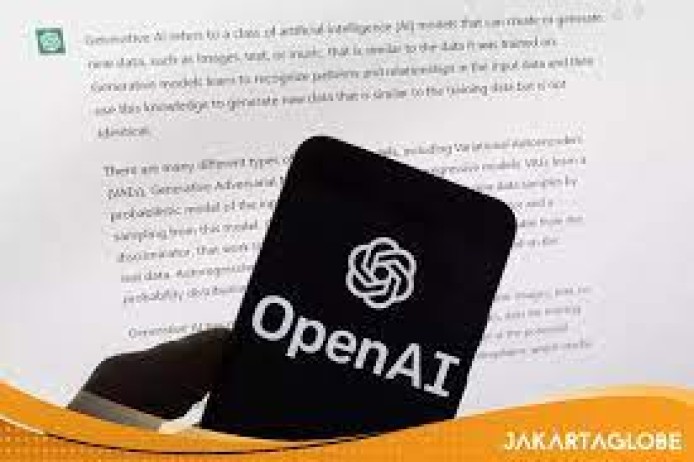
नई दिल्ली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते दायरे और उसकी तेज़ी से बदलती भूमिका पर नया दृष्टिकोण दिया है. नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा प्रकाशित इस अध्ययन में ड्यूक यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड और ओपनएआई के शोधकर्ताओं और अर्थशास्त्रियों ने मिलकर दुनिया के सबसे लोकप्रिय चैटबॉट चैटजीपीटी के वास्तविक उपयोग और प्रभाव का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया है. रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 तक चैटजीपीटी ने साप्ताहिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा 70 करोड़ से पार कर लिया है. यह संख्या दुनिया की वयस्क आबादी के लगभग 10 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है. इन उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रतिदिन औसतन ढाई अरब से अधिक संदेश भेजे जाते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यह “वैश्विक प्रसार की अभूतपूर्व गति” है और इसका प्रभाव अब केवल तकनीकी जिज्ञासा भर नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से गंभीर अध्ययन का विषय बन चुका है.
रिपोर्ट यह भी दिखाती है कि शुरुआती दिनों की तुलना में चैटजीपीटी के उपयोगकर्ताओं की जनसांख्यिकी में भारी बदलाव आया है. आरंभ में इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले लगभग अस्सी प्रतिशत लोग पुरुष थे, लेकिन समय के साथ यह लैंगिक असमानता पूरी तरह से समाप्त हो गई. 2025 के मध्य तक स्त्रीलिंग नाम वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या पुल्लिंग नाम वाले उपयोगकर्ताओं से हल्की बढ़त पर पहुँच गई. इसका अर्थ है कि अब चैटजीपीटी ने लिंग की सीमाओं को पार कर लिया है और यह व्यापक अपील रखने वाला उपकरण बन गया है.
आयु वर्ग के आंकड़े भी दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं. अध्ययन के अनुसार अठारह से पच्चीस वर्ष की आयु वाले युवा उपयोगकर्ताओं का हिस्सा लगभग आधा है और यही वर्ग सबसे अधिक संदेश भेज रहा है. डिजिटल तकनीक के साथ पले-बढ़े ये युवा चैटजीपीटी जैसे एआई टूल्स को अपने रोज़मर्रा के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बना चुके हैं. विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरह यह पीढ़ी शिक्षा, संवाद, मनोरंजन और व्यक्तिगत सहायता के लिए चैटजीपीटी का इस्तेमाल कर रही है, उससे आने वाले समय में एआई और भी गहराई से सामाजिक ढांचे में समाहित हो जाएगा.
अध्ययन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि चैटजीपीटी ने तकनीक तक पहुँच को वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक बना दिया है. रिपोर्ट के अनुसार निम्न और मध्यम आय वाले देशों में उपयोगकर्ताओं की वृद्धि दर विकसित राष्ट्रों की तुलना में कहीं अधिक तेज़ रही है. इसका अर्थ है कि एआई उपकरण अब केवल उच्च आय वर्ग या तकनीक-समझ वाले देशों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि विकासशील समाजों तक भी पहुँच बना चुके हैं. इस प्रवृत्ति को तकनीकी असमानता को कम करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है क्योंकि इससे गरीब और अमीर दोनों ही वर्गों को समान रूप से जानकारी, सहायता और अवसर मिल रहे हैं.
चौंकाने वाली बात यह भी है कि शुरुआत में जहां चैटजीपीटी को मुख्य रूप से कार्यस्थल की उत्पादकता बढ़ाने वाले औज़ार के रूप में देखा जा रहा था, वहीं यह अध्ययन बताता है कि इसका वास्तविक उपयोग कहीं अधिक व्यापक है. लोग अब इसे व्यक्तिगत जीवन के विविध कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं—जैसे शिक्षा में मार्गदर्शन लेना, स्वास्थ्य संबंधी सामान्य जानकारी प्राप्त करना, भाषा सीखना, यात्रा की योजना बनाना, या फिर रोज़मर्रा की छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान खोजना. इसने यह मिथक तोड़ दिया है कि एआई केवल ऑफिस या कार्यक्षेत्र की दक्षता बढ़ाने तक सीमित रहेगा. इसके बजाय यह हर आम व्यक्ति का व्यक्तिगत सहायक बनता जा रहा है.
शोधकर्ताओं का कहना है कि यह बदलाव समाज में एआई की भूमिका को लेकर स्थापित धारणाओं को चुनौती देता है. अब यह केवल पेशेवर कार्यों को आसान बनाने वाला उपकरण नहीं बल्कि जीवनशैली और दैनिक दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुका है. यही कारण है कि नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अर्थशास्त्रियों को इसके दीर्घकालिक प्रभावों को समझने और उनका आकलन करने की तत्काल आवश्यकता है.
रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि इतनी तेज़ी से फैल रही तकनीक के साथ अवसरों के साथ-साथ चुनौतियाँ भी आती हैं. डेटा गोपनीयता, गलत सूचनाओं का प्रसार, और एआई पर बढ़ती निर्भरता जैसे मुद्दों पर समाज को गंभीरता से विचार करना होगा. लेकिन सकारात्मक दृष्टि से देखें तो चैटजीपीटी ने यह साबित कर दिया है कि एआई केवल अभिजात वर्ग का उपकरण नहीं बल्कि वैश्विक जनसाधारण की पहुँच में भी आ सकता है.
इस अध्ययन को भविष्य की नीतियों और तकनीकी ढांचे को तैयार करने में अहम माना जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि 10 प्रतिशत वयस्क आबादी पहले ही इस तकनीक को अपना चुकी है, तो आने वाले वर्षों में यह अनुपात दोगुना या तिगुना भी हो सकता है. शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, और व्यक्तिगत जीवन—हर क्षेत्र में इसके गहरे असर की संभावना है.
आख़िरकार यह निष्कर्ष निकलता है कि चैटजीपीटी अब किसी एक देश, वर्ग या क्षेत्र की सीमाओं में बंधा नहीं रहा. यह तकनीक का वैश्विक चेहरा बन चुका है जिसने कुछ ही वर्षों में संवाद और जानकारी के आदान-प्रदान का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. एनबीईआर की यह रिपोर्ट न केवल एआई की वर्तमान स्थिति का चित्रण करती है बल्कि भविष्य की झलक भी दिखाती है कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव समाज की संरचना को पुनर्परिभाषित करने जा रही है.